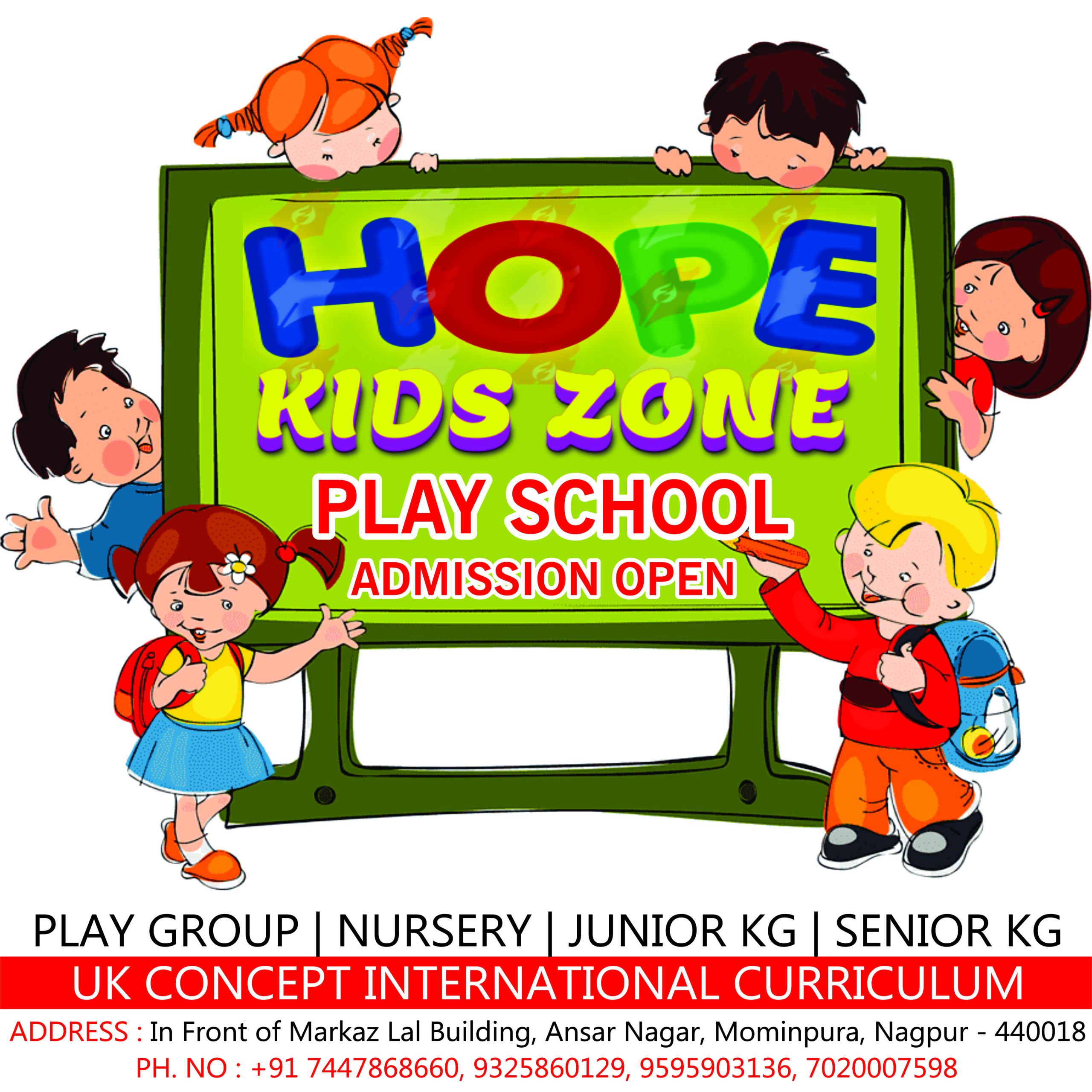नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच संबंधों को बदलने के लिए दो दशकों से भी ज़्यादा समय से चल रहे द्विदलीय प्रयासों के बाद, जिसमें उनका अपना पहला कार्यकाल भी शामिल है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब इस कड़ी मेहनत से बनाए गए रिश्ते को खत्म करने की प्रक्रिया में हैं।
भारत के साथ व्यापार वार्ता रोक दी और (सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए) 25 प्रतिशत का बेसलाइन टैरिफ़ लगा दिया, जबकि चीन को एक और विस्तार दिया—“दोस्त” और प्रतिद्वंद्वी के बीच का यह अंतर नई दिल्ली में किसी से छिपा नहीं है।
4 अगस्त को घोषणा की गई कि वह 25 प्रतिशत टैरिफ़ को और बढ़ाएगा और रूस से भारत की तेल ख़रीद पर अतिरिक्त दंड लगाएगा। इस कदम को नई दिल्ली में एक ज़बरदस्त दबाव, भारतीय विदेश नीति में घोर हस्तक्षेप, भारत की तेल आयात ज़रूरतों को देखते हुए अव्यावहारिक, और यूक्रेन के ख़िलाफ़ मास्को को युद्ध रोकने के लिए राज़ी करने में पश्चिम (और ट्रंप की अपनी) सामूहिक विफलता के लिए “भारत को दोष देने” का एक निंदनीय प्रयास माना जाएगा।
ब्राज़ील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों के साथ ब्रिक्स समूह में भारत की भागीदारी के लिए उस पर और भी अधिक टैरिफ लगाने की धमकी दी। आश्चर्य की बात नहीं कि नई दिल्ली इसे भी घोर हस्तक्षेप और दबाव के रूप में देखती है।
भारत में विनिर्माण करने वाली अमेरिकी कंपनियों की आलोचना की और उन्हें धमकाया—जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की एक प्रमुख प्राथमिकता है—साथ ही उन्हें अमेरिका में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया, अन्यथा वित्तीय दंड का सामना करना पड़ेगा। इसने ट्रम्प के “अमेरिका फ़र्स्ट” और मोदी के “मेक इन इंडिया” दृष्टिकोण के बीच सहज और अंतर्निहित विरोधाभास को और बढ़ा दिया है।
भारत पर आतंकवादी हमले के कुछ हफ़्तों के भीतर ही व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के सेना प्रमुख के साथ घुलमिल गए, जबकि इस्लामाबाद को केवल 19 प्रतिशत की बेहतर टैरिफ दर और पाकिस्तान के तेल भंडारों का संयुक्त रूप से अन्वेषण करने का वचन दिया।
एक नए अमेरिकी तकनीकी राष्ट्रवाद का ढिंढोरा पीटना जारी रखा, जिसमें विदेशियों के साथ प्रौद्योगिकी साझा करने को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। राष्ट्रपति के आसपास के कुछ लोगों की प्रवृत्ति अमेरिकी प्रौद्योगिकी को अपने ही देश में रखने और विदेशी साझेदारों के साथ निर्यात और सह-नवाचार को कम करने की है।
भारत के खिलाफ ट्रंप की धमकियों को खारिज करना निश्चित रूप से आसान है, और अनुभवी लोग पाँच आधारों पर ऐसा कर रहे हैं
पहला
जैसा कि पूर्व सहायक वाणिज्य सचिव रे विकरी ने कहा है, राष्ट्रपति सौदे करने से पहले बड़बोलेपन का परिचय देते हैं, इसलिए किसी समय ट्रंप के “व्यापार समझौते” से भारत की 25 प्रतिशत आधारभूत टैरिफ दर कम होने की संभावना है।
दूसरा
जैसा कि मेरे कार्नेगी सहयोगी रुद्र चौधरी ने सही लिखा है, अमेरिकियों और भारतीयों के बीच वाणिज्यिक, तकनीकी और सामाजिक संबंधों का पारिस्थितिकी तंत्र ट्रंप से भी गहरा है, जिसमें अरबों डॉलर का दोतरफा निवेश है, कई तकनीकी कंपनियाँ एक साथ काम कर रही हैं, और हज़ारों भारतीय और अमेरिकी इंजीनियर और उद्यम पूँजीपति एक-दूसरे के साथ गहन रूप से जुड़े हुए हैं।
तीसरा
जैसा कि प्रमुख रणनीतिक मामलों के विश्लेषक सी. राजा मोहन कहते हैं, भारत को संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है, इसलिए ट्रंप की कठोर रणनीति भारत को फिर से संगठित होने के लिए प्रेरणा भी प्रदान कर सकती है।
चौथा
जैसा कि हडसन इंस्टीट्यूट के वाल्टर रसेल मीड सुझाव देते हैं, कुछ स्थायी, स्थायी और शायद स्थायी “दर्दनाक बिंदु” हैं जिन्होंने सबसे अच्छे समय में भी द्वेष पैदा किया है और सहयोग में बाधाएँ खड़ी की हैं।
वास्तविक दुनिया में, भू-राजनीतिक खतरे अभी भी मायने रखते हैं, इसलिए विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने चीनी शक्ति के उदय के बारे में जिन साझा चिंताओं की पहचान की है, वे निश्चित रूप से कुछ रणनीतिक अभिसरण उत्पन्न करेंगी।
लेकिन ये चेतावनियाँ दो सबसे बुनियादी तथ्यों की अनदेखी करती हैं: घरेलू राजनीति लगभग हमेशा विदेश नीति पर भारी पड़ती है, और विदेश नीति के तर्क लगभग कभी भी तब तक प्रभावी नहीं होते जब तक कि वे एक मज़बूत घरेलू राजनीतिक आधार पर आधारित न हों।
चीन के साथ अमेरिकी वाणिज्यिक
तकनीकी और सामाजिक संबंध भारत की तुलना में कहीं अधिक गहरे हो गए हैं। फिर भी, चार दशकों के घातीय विकास और गहरे संबंधों के बाद, बदलती रणनीतिक गणनाओं और बदली हुई घरेलू राजनीति के बीच, ये संबंध कुछ ही वर्षों में तेज़ी से बिखर गए हैं।
उल्लेखनीय रूप से, और दो दशकों में पहली बार, ट्रम्प के कार्यों, बयानों और दबावपूर्ण लहजे ने भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों को एक ज्वलंत घरेलू राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। विपक्ष, मीडिया और भारतीय जनता ने ट्रम्प की धमकियों के सामने कमज़ोरी दिखाने से बचने के लिए सरकार को चेतावनी दी है।
और यह देखते हुए कि अमेरिकी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा ट्रम्प के साथ जहाँ भी जाता है, चलता है, क्या भारत के साथ संबंधों को अमेरिकी घरेलू राजनीति में एक फुटबॉल बनने में ज़्यादा समय लग सकता है? वाशिंगटन में भारत से सीधे जुड़े मुद्दे सबसे ज़्यादा पक्षपातपूर्ण और विस्फोटक हैं, जिनमें आव्रजन और निर्वासन, तकनीकी कर्मचारियों के लिए H1B वीज़ा, अमेरिकी कंपनियों द्वारा विदेश में विनिर्माण और विदेश में उत्पादन, और विदेशियों के साथ तकनीक साझाकरण और सह-नवाचार शामिल हैं।यह अमेरिका-भारत संबंधों के अगले दो दशकों के लिए अशुभ संकेत है, क्योंकि 2000 के दशक के पहले दशक के बाद से घरेलू राजनीति और पक्षपात पर काबू पाना शायद सबसे बड़ी उपलब्धि रही है।
और पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के प्रशासन के अंत में अमेरिका-भारत संबंधों की देखरेख करने वाले अमेरिकी उप-सहायक विदेश मंत्री के रूप में, मैं व्यक्तिगत रूप से यह प्रमाणित कर सकता हूँ कि पक्षपात, राजनीतिकरण और इतिहास के बोझ तले दबे इस माहौल से उबरने के लिए दोनों देशों के बहुत से लोगों ने कड़ी मेहनत की है। वास्तव में, पिछली बार जब घरेलू राजनीति ने अमेरिका-भारत संबंधों के परिवर्तन को लगभग पटरी से उतार दिया था, वह इसी अवधि के दौरान था।
जुलाई 2008 में, वाशिंगटन के साथ 2005 के ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौते पर तीन साल तक अड़चन डालने के बाद, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार अविश्वास प्रस्ताव लगभग हार गई थी, जब गठबंधन के बाहर से सरकार का समर्थन कर रहे वाम मोर्चे ने समझौते पर अपना समर्थन वापस ले लिया। भारतीय राजनीति बिखर गई। और विडंबना यह है कि जिन दलों ने लंबे समय से अमेरिका-भारत के घनिष्ठ संबंधों का समर्थन किया था, उन्होंने सरकार को गिराने के लिए उसके खिलाफ मतदान किया। सिंह बच गए, और समझौता आगे बढ़ा—लेकिन केवल यूपीए गठबंधन के बाहर के दलों, जैसे समाजवादी पार्टी, जो उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश में एक मज़बूत पकड़ रखने वाली क्षेत्रीय पार्टी है, के वोटों के कारण।
आज, अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी की वाह-वाही करने वालों में से बहुत कम लोग यह याद रखते हैं कि परमाणु समझौता कितने करीब से टूटने के कगार पर था। लेकिन ये दो सबक स्पष्ट हैं: एक बार जब घरेलू राजनीति आड़े आती है, तो अच्छे इरादे और अच्छे विचार विफल हो सकते हैं; और विश्वास बनाना मुश्किल होता है, उसे बनाए रखना और भी मुश्किल, और सबसे मुश्किल तो तब होता है जब वह राजनीतिकरण के दलदल में धंस जाता है।
अमेरिका-भारत संबंध अब, खासकर नई दिल्ली में, एक राजनीतिक फुटबॉल बन सकते हैं। और जिन बुनियादी समझों ने अमेरिका-भारत संबंधों को और मज़बूत बनाया था, वे भी गंभीर खतरे में पड़ सकते हैं:
नई दिल्ली ने मोटे तौर पर यह मान लिया था कि वाशिंगटन संबंधों को मज़बूत करने के लिए राजनीतिक जोखिम उठाएगा। ट्रंप ने ऐसा नहीं किया है और ज़ाहिर है कि वे ऐसा नहीं करेंगे।
पाकिस्तान के मुद्दे पर अमेरिका और भारत के बीच अक्सर मतभेद रहे हैं, लेकिन वाशिंगटन नई दिल्ली के हितों के प्रति संवेदनशील रहा है और उसने अमेरिकी नीतियों को उसी के अनुसार ढालने की कोशिश की है। ट्रंप द्वारा इस्लामाबाद की भरपूर प्रशंसा और पाकिस्तानी सेना व सरकार के साथ समझौते अब नई दिल्ली में स्पष्ट चिंताएँ पैदा करते हैं कि यह भी अब पीछे छूट गया है। और ये चिंताएँ और भी बढ़ गई हैं क्योंकि ट्रंप के ये कदम 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के कुछ ही हफ़्तों के भीतर आए हैं, जिसमें छब्बीस भारतीय नागरिक मारे गए थे और दोनों देशों के बीच शत्रुता का एक नया दौर शुरू हो गया था।
दोनों देशों ने तीसरे पक्षों के साथ एक-दूसरे के इरादों पर भरोसा नहीं किया, लेकिन यह सीख लिया कि इसे घनिष्ठ संबंधों में बाधा नहीं बनाना चाहिए। नई दिल्ली, बीजिंग और इस्लामाबाद के साथ वाशिंगटन के समझौते को लेकर चिंतित थी। ईरान, म्यांमार और बाद में रूस के साथ भारत के संबंधों ने अमेरिका को परेशान कर दिया था। ट्रंप और उनका प्रशासन अब रूस के साथ तेल व्यापार को लेकर भारत पर प्रतिबंध और टैरिफ लगाने की ओर बढ़ रहा है। इससे द्विपक्षीय संबंधों के मानदंड में महत्वपूर्ण बदलाव आया है।
लंबे समय से चले आ रहे अविश्वास के बावजूद, दोनों पक्षों ने अपनी भाषा और लहजे में संयम बरता। ट्रंप ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि भारत की आलोचना की और उसे “मृत अर्थव्यवस्था” तक कह डाला।
दोनों पक्षों और सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने एक द्विदलीय आधार सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की। इसलिए यह विडंबना ही है कि कांग्रेस पार्टी, जिसने 2005 में वाशिंगटन के साथ परमाणु समझौते का नेतृत्व किया था, अब नई दिल्ली में अमेरिका-भारत संबंधों की आलोचना का नेतृत्व कर रही है, जबकि बुश की रिपब्लिकन पार्टी के उत्तराधिकारी लगभग रोज़ाना सोशल मीडिया पर भारत की आलोचना कर रहे हैं।
जो लोग सोचते हैं कि अमेरिका और भारत को बहुत कुछ हासिल होगा और टूटने से उन्हें और भी अधिक नुकसान होगा, उनके लिए अमेरिका-भारत संबंधों का राजनीतिकरण एक धीमी गति वाली आपदा है।